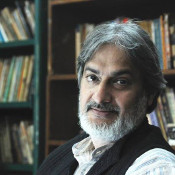साइलेन्स, लाइट्स, रोल साउन्ड, रोल कॅमरा ऍन्ड ऍक्शन... कट इट... शॉट ओके... लेकिन एक टेक और लेते हैं।
ये दुनिया है सिनेमा की, जो अब शतायु हो चुका है हमारे देश में...
क्या-क्या हो लिया इन सौ सालों में…?
सिनेमा का सफ़र एक वैज्ञानिक आविष्कार से शुरू हुआ और मनोरंजन का साधन बनने के बाद आज संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गया है। जो लोग ये सोचते थे कि सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन के लिए ही है, वे ग़लत साबित हुए। जिस तरह साहित्य, कला, विज्ञान और संगीत की एक श्रेणी मनोरंजन ‘भी’ है, उसी तरह सिनेमा भी सिर्फ़ मनोरंजन 'ही' नहीं है।
ख़ैर... सिनेमा ने वक़्त-वक़्त पर अनेक रूप रखे हैं। सिनेमा को नाम भी तमाम दिए गए, जैसे- कला फ़िल्म, समांतर सिनेमा, सार्थक सिनेमा, मसाला फ़िल्म आदि–आदि। लेकिन एक नाम बिल्कुल सही है, वो है ‘सार्थक सिनेमा’। जो फ़िल्म जिस उद्देश्य से बनी है, यदि वह पूरा हो रहा है तो वह फ़िल्म सार्थक फ़िल्म है। वही सफल सिनेमा है।
शुरुआती दौर मूक फ़िल्मों का था। भारत में 1913 में दादा साहब फाल्के के भागीरथ प्रयासों से 'राजा हरिश्चंद्र' पहली फ़ीचर फ़िल्म रिलीज़ हुई। चार्ली चॅपलिन, जिन्हें विश्व सिनेमा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ने एक से एक बेहतरीन फ़िल्म इस दौर में बनाईं जैसे- मॉर्डन टाइम्स, सिटी लाइट्स, गोल्ड रश, द किड आदि। इस दौर में रूसी निर्देशक सर्गेई आइसेंसटाइन की फ़िल्म 'बॅटलशिप पोटेम्किन' सन 1926 में आई। इस फ़िल्म का एक मशहूर दृश्य, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को बग्घी में सीढ़ियों पर ले जा रही है, बहुत मशहूर हुआ। जिसको ‘डि पामा’ ने अपनी फ़िल्म ‘अनटचेबल’ (1987) में भी फ़िल्म के अंतिम दृश्य में इस्तेमाल करके आइंसटाइन को श्रद्धांजलि दी।
1931 में 'आलम आरा' के रिलीज़ होने से 'सवाक' याने बोलती हुई फ़िल्मों का दौर शुरू हो गया था। टॉकीज़ के शुरुआती दौर में, अशोक कुमार और देविका रानी अभिनीत 'अछूत कन्या' (1936) ने अपनी अच्छी पहचान बनाई। यह द्वितीय विश्वयुद्ध का समय था। इस समय 'चार्ली चॅपलिन' की फ़िल्म 'द ग्रेट डिक्टेटर' आई। इस फ़िल्म में उन्होंने मानवता पर एक बेहतरीन भाषण दिया है। चार्ली चॅपलिन को जगह-जगह इस भाषण के लिए बुलाया जाता था जिससे कि लोग मानवता का पाठ सीखें। 5-6 मिनट के इस भाषण को बोलने में चॅपलिन को कई बार बीच में ही पानी पीना पड़ा क्योंकि भाषण इतना भावुकता से भरा था कि गला अवरुद्ध हो जाता था। जनता पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। आज भी यह भाषण यादगार है।
1939 में ‘गॉन विद द विंड’ ने क्लार्क गॅबल को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। इस फ़िल्म ने लागत से सौ गुनी कमाई की। अब फ़िल्मों के लिए बजट कोई समस्या नहीं रह गई थी। बाद में ‘बेन-हर’ (1959) ने भी यह साबित कर दिखाया कि बहुत महंगी फ़िल्में यदि गुणवत्ता से बिना समझौता किए बनाई जाएं तो उनकी कमाई सिनेमा उद्योग को पूरी तरह स्थापित और मज़बूत करने में सहायक होती है। इटली और फ़्रांस ने बहुत उम्दा फ़िल्में विश्व को दी हैं। 1948 में इटली के वितोरियो दि सिका की ‘बाइस्किल थीव्स’ एक बेहतरीन फ़िल्म साबित हुई। सारी दुनिया में इसकी सराहना हुई और फ़िल्मों को केवल मनोरंजन का साधन न मानते हुए संस्कृति और समाज के दर्पण के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।
प्यार-मुहब्बत के विषय पर हॉलीवुड में 'कासाब्लान्का' (1942) फ़िल्म को एक अधूरी प्रेम कहानी की बेजोड़ प्रस्तुति माना गया। इस फ़िल्म ने इंग्रिड बर्गमॅन को अभिनेत्री के रूप में सिनेमा-आकाश के शिखर पर पहुँचा दिया। इंग्रिड बर्गमॅन ने ढलती उम्र में इंगार बर्गमॅन की स्वीडिश फ़िल्म 'ऑटम सोनाटा' (1978) में भी उत्कृष्ट अभिनय किया। यह फ़िल्म दो व्यक्तियों के परस्पर संवाद, अंतर्द्वंद, पश्चाताप, आत्मस्वीकृति, आरोप-प्रत्यारोप का सजीवतम चित्रण थी। इसी दौर में वहीदा रहमान अभिनीत 'ख़ामोशी' (1969) आई, जिसने वहीदा रहमान को भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बना दिया। वहीदा रहमान के अभिनय की ऊँचाई हम 'प्यासा' में देख चुके थे।
'प्यासा' (1957) गुरुदत्त ने बनाई थी। गुरुदत्त सिनेमा जगत में लाइटिंग इफ़ॅक्ट के लिए विश्वविख्यात हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए 'सॉंग पिक्चराइज़ेशन' भी कमाल के हैं। सॉंग पिक्चराइज़ेशन के लिए विजय आनंद बॉलीवुड सिनेमा में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। उन्होंने फ़िल्म निर्देशन में जो प्रयोग किए हैं, वो ग़ज़ब हैं। 'गाइड' का गाना 'आज फिर जीने की तमन्ना है' मुखड़े की बजाय अंतरे से शुरू है और 'ज्यूल थीफ़' (1967) का गाना 'होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई' में विजय आनंद का निर्देशन और वैजयंती माला का नृत्य अभी तक बेजोड़ माना जाता है।
यश चौपड़ा ने प्रेम त्रिकोण को अपना प्रिय विषय बना लिया तो ऋषिकेश मुखर्जी ने स्वस्थ कॉमेडी को। ऋषिकेश मुखर्जी ने फ़िल्म सम्पादन से अपनी शुरुआत की थी। दोनों ने ही विदेशी फ़िल्मों की नक़ल करने के बजाय अधिकतर भारतीय मौलिक कहानियों को चुना।
1954 में जापानी फ़िल्म 'द सेवन समुराई' बनी, जो 'अकीरा कुरोसावा' ने बनाई। जापान के अकीरा कुरोसावा 'विश्व सिनेमा जगत के पितामह' कहे जाते हैं। विश्व की श्रेष्ठ फ़िल्मों में गिनी जाने वाली इस फ़िल्म को आधार बना कर अनेक फ़िल्में बनी जिनमें एक रमेश सिप्पी की 'शोले' भी है। अल्पायु में ही स्वर्ग सिधारे जापान के महान कहानीकार 'रुनोसुके अकूतगावा' की दो कहानियों पर आधारित अद्भुत फ़िल्म, 'राशोमोन' बना कर कुरोसावा पहले ही ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इस समय भारत में भी कई अच्छी फ़िल्में बनीं। सत्यजित राय, 'पाथेर पांचाली' (1955) बना रहे थे, जिसकी शूटिंग के लिए बार-बार पैसा ख़त्म हो जाता था लेकिन अपने पसंदीदा 40 एम.एम. लेन्स के साथ उन्होंने इस फ़िल्म से भारत में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में शोहरत पाई। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि कुरोसावा ने सत्यजित राय के लिए कहा-
"सत्यजित राय के बिना सिनेमा जगत वैसा ही है जैसे सूरज-चाँद के बिना आसमान।"
सत्यजित राय ने राजकपूर की 'मेरा नाम जोकर' के प्रथम भाग (बचपन वाला) को 10 महान फ़िल्मों में से बताया। राजकपूर अभिनीत 'जागते रहो' (1956) और महबूब ख़ान की 'मदर इंडिया' (1957) जैसी अच्छी फ़िल्में आईं। 1957 में ही एक और अच्छी फ़िल्म ‘दो आंखें बारह हाथ’ वी. शांताराम ने बनाई। ये सिनेमा 1980-90 तक आते-आते श्याम बेनेगल की 'अंकुर' और गोविन्द निहलानी की 'आक्रोश' भी हमें दिखा गया और 'रिचर्ड एटनबरो' की महात्मा गाँधी पर बनी उत्कृष्ट फ़िल्म 'गांधी' भी।
रहस्य-रोमांच और डर का विषय भी सिनेमा में ख़ूब चला। 'अल्फ़्रेड हिचकॉक' इसके विशेषज्ञ थे। उन्होंने तमाम फ़िल्में इसी विषय पर बनाईं जैसे- द 39 स्टेप्स, डायल एम फ़ॉर मर्डर, वर्टीगो आदि, लेकिन 'साइको' उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। दुनिया भर में हिचकॉक की फ़िल्मों की और दृश्यों की नक़ल हुई।
हॉलीवुड में 'वॅस्टर्न्स' (काउ बॉय कल्चर वाली फ़िल्में) का ज़ोर भी चल निकला। सरजो लियोने की 'वंस अपॉन ए टाइम इन द वॅस्ट' एक श्रेष्ठ फ़िल्म बनी। सरजो लियोने ने क्लिंट ईस्टवुड के साथ कई फ़िल्में बनाईं। इन फ़िल्मों में 'ऐन्न्यो मोरिकोने' के संगीत दिया और सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। 'नीनो रोटा' भी फ़िल्मों में लाजवाब संगीत दे रहे थे जिसका इस्तेमाल इटली के फ़िल्मकारों ने ख़ूब किया।
फ़ॅदरिको फ़ॅलिनी ने 1963 में 81/2 फ़िल्म बनाई तो वह विश्व की दस सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मों में जगह पा गई। इस फ़िल्म में संगीत 'नीनो रोटा' ने ही दिया और फ़िल्म की पकड़ इतनी ज़बर्दस्त बनी कि हम फ़िल्म से ध्यान हटा ही नहीं सकते। फ़ोर्ड कॉपोला ने भी 'मारियो पुज़ो' के उपन्यास पर आधारित फ़िल्म 'द गॉडफ़ादर' के लिए 'नीनो रोटा' को ही चुना। फ़िल्मों में अच्छे संगीत की भूमिका अब प्रमुख हो गई। संगीत के बादशाह 'मोत्ज़ार्ट' पर माइलॉस फ़ोरमॅन ने 'अमादिउस' बनाई। वुल्फ़गॅन्ग अमादिउस मोत्ज़ार्ट और अन्तोनियो सॅलिरी की कहानी पर बनी यह फ़िल्म, फ़ोरमॅन के उस करिश्मे से बड़ा करिश्मा थी, जो वे 1975 में 'वन फ़्ल्यू ओवर द कुक्कूज़ नेस्ट' बना कर कर चुके थे।
पचास के दशक में के.आसिफ़ ने मशहूर फ़िल्म 'मुग़ल-ए-आज़म' शुरू की, जो क़रीब नौ साल का समय लेकर 1960 में प्रदर्शित हुई। यूँ तो मुग़ल-ए-आज़म से जुड़े हुए हज़ार अफ़साने हैं, लेकिन उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ का ठुमरी गाने का अंदाज़ सबसे रोचक है। इस फ़िल्म के संगीतकार नौशाद, के. आसिफ़ को लेकर बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ के घर पहुँचे और उनसे फ़िल्म में गाने के लिए कहा। बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ ने दोनों को टालने के लिए 25 हज़ार रुपये मांगे क्योंकि उस समय फ़िल्मों में गाना शास्त्रीय गायकों के लिए ओछी बात मानी जाती थी। के. आसिफ़ को चुटकी बजाकर बात करने की आदत थी, उन्होंने चॅक बुक निकालकर 10 हज़ार की रक़म लिखी और ख़ाँ साहब को चॅक थमा दिया और चुटकी बजाकर बोले "ये लीजिए एडवांस मैं आपको 25 हज़ार ही दूँगा।" पचास के दशक में फ़िल्मों में गाना गाने के हज़ार, दो हज़ार रुपये मिला करते थे।
आख़िरकार बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे। वहाँ उन्होंने औरों की तरह खड़े होकर गाने से मना कर दिया तो ज़मीन पर गद्दा, चांदनी और मसनद की व्यवस्था की गई। इतने पर भी ख़ाँ साहब गाने को राजी न हुए और उन्होंने पहले उस दृश्य को फ़िल्माने के लिए कहा, जिस पर कि उनकी ठुमरी चलनी थी। इसके बाद दिलीप कुमार और मधुबाला का वो दृश्य फ़िल्माया गया, जिसमें दिलीप कुमार, मधुबाला के चेहरे पर पंख से हल्के-हल्के से सहला रहे हैं। यह दृश्य स्टूडियो में पर्दे पर प्रोजेक्टर से चलाया गया और इसको देखते हुए ख़ाँ साहब ने अपनी मशहूर ठुमरी गायी। राग सोहणी में ‘प्रेम जोगन बनके’ ठुमरी, जितनी बार भी सुन लें, अच्छी ही लगती है। ठुमरी गा कर ख़ाँ साब बोले-
"वैसे ये लड़का और ये लड़की हैं तो अच्छे..."
इस सप्ताह इतना ही... अगले सप्ताह कुछ और...
-आदित्य चौधरी
संस्थापक एवं प्रधान सम्पादक